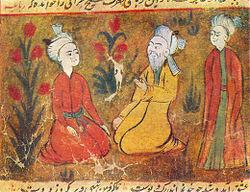शीर्ष प्रश्न
समयरेखा
चैट
परिप्रेक्ष्य
आदिकाल
हिन्दी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक का काल विकिपीडिया से, मुक्त विश्वकोश
Remove ads
आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारम्भिक चरण है, जिसका समय 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी (1050 से 1375 विक्रम संवत्) तक माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह युग विकेंद्रीकरण की ओर जा रहा था। सम्राट् हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात् भारतवर्ष में केंद्रीयता की भावना प्रायः लुप्त हो चुकी थी और देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था। इन छोटे राज्यों के राजा ज़रा-ज़रा सी बात पर आपस में युद्ध करते रहते थें। दूसरी तरफ़ देश पर बाह्य आक्रांताओं के निरंतर आक्रमण हो रहे थें। देश का वातावरण भारी हलचल और अशांति से भरा हुआ था।[1][2][3][4][5][6][7]
Remove ads
आदिकाल के नामकरण की समस्या
सारांश
परिप्रेक्ष्य
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आदिकाल सदा से विद्वानों के बीच विवाद का विषय रहा है। चाहे इसके नामकरण की बात हो या काल-विभाजन की, आदिकाल को लेकर इतिहासकारों व विद्वानों के मध्य पर्याप्त मतभेद मिलते हैं क्योंकि आदिकाल के इतिहास का समुचित पर्यालोचन करने में इतिहासकारों व विद्वानों को कठिनाई होती है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस समय के कुछ ग्रंथ अप्राप्य हैं तो कुछ रचनाओं पर प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता का सवाल लगा हुआ है, वहीं कुछ ग्रंथों में ऐतिहासिक सामंजस्य का अभाव है। साथ ही इस युग में धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में परस्पर विरोधी तत्व दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक विशेष तत्व को ध्यान में रखकर इसका नाम निर्धारित कर देना उचित नहीं।[8][9][10][5] इस संबंध में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा हैं कि
शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े-बड़े कवि उत्पन्न हुए, जिनकी रचनाएँ अलंकृत काव्य-परम्परा की चरम सीमा पर पहुँच गई थीं और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए, जो अत्यन्त सहज-सरल भाषा में, अत्यन्त संक्षिप्त शब्दों में, अपने मार्मिक मनोभाव प्रकट करते थें।.... संक्षेप में इतना जान लेना यहाँ पर्याप्त है कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है और इसीलिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।[11]
विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के अलग-अलग नाम सुझाए हैं, जो इस प्रकार है-
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों (विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक-जस-चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली) के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया था।
- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल की संज्ञा दी।
- जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को चारण कवियों को ध्यान में रखकर चारणकाल कहा।
- डॉ॰ रामकुमार वर्मा ने जॉर्ज ग्रियर्सन की ही तरह इस काल को चारणकाल कहा। साथ ही उन्होंने इस काल को संधिकाल भी कहा।
- महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल नाम से संबोधित किया।
- राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया।
- मिश्र बंधुओं ने इस काल को पूर्व प्रारंभिक काल कहा।
- डॉ॰ गणपति चंद्र गुप्त ने इस काल को शून्य काल कहा।
- धीरेंद्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस काल को अपभ्रंश काल नाम दिया।
- विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीरकाल के नाम से संबोधित किया।
- राम शंकर शुक्ल 'रसाल' ने इस काल को बाल्यावस्था काल की संज्ञा दी।
- मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इस काल को आधार काल कहा।
- पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इस काल को अंधकार काल की संज्ञा दी।
Remove ads
आदिकाल की परिस्थितियाँ
सारांश
परिप्रेक्ष्य
आदिकाल का समय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर दृष्टि से उथल-पुथल का समय था। राजनीतिक स्तर पर जहाँ एक तरफ़ भारत पर निरंतर विदेशी आक्रमण हो रहे थें तो वहीं दूसरी तरफ़ सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में आंतरिक कलह काफ़ी बढ़ गये थें। धार्मिक स्तर पर इस समय तक आते-आते बौद्ध और जैन धर्म में भी काफ़ी बदलाव हुए और हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान जैसी कई धर्म की शाखाएँ निकल गई थी। निरंतर होते इन युद्धों और धार्मिक बदलावों के कारण आम जन-जीवन में भी परिवर्तन हुए। सामान्य जन जहाँ युद्ध के दुष्परिणामों से त्रस्त थीं तो वहीं धार्मिक स्तर पर पनप रहे विभिन्न शाखाओं के भी प्रति उनके मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अतः आदिकालीन समय-साहित्य को समझने के लिए उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति को समझना अतिआवश्यक है।[5][12]
राजनीतिक परिस्थिति
हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात देश में आंतरिक संघर्ष यानी राजपूत राजाओं के आपसी झगड़े और बाहरी आक्रमण काफ़ी बढ़ गए थें। देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये थें। इनमें गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजवंश प्रमुख थें। इन राजवंशों के राजा आपस में प्रायः लड़ा करते थें। इन पारस्परिक युद्धों के लिए यह आवश्यक न था कि कोई विशेष कारण हो। ये लोग अपने प्रभाव की वृद्धि, शौर्य प्रदर्शन अथवा किसी सुंदरी की प्राप्ति हेतु ही आपस में लड़ा करते थें। दूसरी तरफ़ भारत के सिंध आदि पश्चिमी प्रदेशों पर मुस्लिम शासक बहुत दिनों से आक्रमण करते आ रहे थें। उन्होंने सिंध, पंजाब आदि प्रांतों पर आधिपत्य भी कर लिया था और अब वे लोग राजपूताने की ओर बढ़ने लगे थें। भारत का उत्तरापथ भी विदेशियों द्वारा आक्रांत होने लगा था। महमूद गजनवी के आक्रमण का भी यही युग था। मुइज़ुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी ने भी इसी युग में भारत विजय करने के लिए बार-बार आक्रमण किया था। उस वक्त के राजा पृथ्वीराज और जयचंद की पारस्परिक कलह और इसका लाभ उठाते हुए मुइज़ुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी का विजय प्राप्त करना तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का भली प्रकार प्रतिनिधित्व करता है। इस समय के कुछ आक्रमणकारी केवल लूटमार के लिए आए तथा सम्पत्ति लूट कर चले गए और कुछ धर्म-प्रचार की इच्छा से आए जबकि कुछ भारत की सुख-समृद्धि तथा विपुल धन-धान्य से आकृष्ट होकर इस देश पर अधिकार जमाने की धुन में लग गए। तत्कालीन राजपूत राजा कुछ समय तक तो इनसे लड़ते रहें परन्तु संगठित ना होने के कारण और अंतर्कलह से क्षीण होने के कारण वे जल्द सत्ता खो बैठें।[5][13][14][12]
सामाजिक परिस्थिति
राजनीतिक एकता भंग हो जाने के कारण इस युग में गृह कलह बढ़ गये थें और स्वयंवरों में बल-प्रदर्शन करने तक ही तत्कालीन राजाओं की वीरता सीमित हो गई थी। इस समय के भारतीय शासक प्रायः विलासी हो गये थें। युद्ध का वातावरण होने के कारण युद्ध और युद्ध में वीरता के साथ वीरगति प्राप्त करना जन-जीवन का एक अंग बन गया था। माताएँ ऐसे पुत्र की कामना करती थीं जो जन्म लेने के साथ ही तलवार चलाना शुरू कर दें-
हूँ बलिहारी राणियाँ भ्रूण सिखावण भाउ।
नालौ बाडर री छुरी झपट्यौ जाण्यो साउ॥[15]
इस युग के स्त्री समाज में सती और जौहर की प्रथा व्यापक रूप से व्याप्त थी। युद्ध में पराजय हो जाने पर पत्नियाँ पति के साथ सती हो जाती थीं अथवा सामूहिक रूप से जौहर कर लेती थीं। कई पत्नियाँ तो युद्ध में जाते समय झिझक एवं मोह दिखाने वाले पतियों के सम्मुख अपना सिर काटकर रख दिया करती थीं।[5][13][14][7][12]
धार्मिक परिस्थिति
आदिकाल का समय धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही उथल-पुथल का समय था। बौद्ध और जैन धर्मों में आंतरिक मतभेद के कारण विविध शाखाएँ निकल गई थीं। जहाँ एक ओर सम्राट हर्षवर्धन के समय में ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों का समान आदर था। हर धर्म के प्रति एक उदार और धार्मिक सहिष्णुता की भावना व्याप्त थी, आपसी मेल-जोल था। वहीं हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात केन्द्रीय सत्ता के अभाव में जब देश खंड राज्यों में विभक्त हो गया तो धीरे-धीरे धर्म के क्षेत्र में भी अराजकता फैल गयी। वेद-शास्त्रों के विधि-विधान और कर्म-काण्ड को लेकर चलने वाले ब्राह्मण धर्म तथा बौद्ध धर्म में भी संघर्ष होने लगे। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय अपने पवित्र रूप को सुरक्षित न रख सके और आंतरिक विवाद के कारण विकृत होकर नये-नये रूपों में जनता के सामने आने लगें। हीनयान, वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान आदि की उत्पत्ति के पीछे का यही कारण है। परिणामतः आम आदमी धर्म के वास्तविक आदर्श को भूलकर जादू-टोना और तंत्र-मंत्र में विश्वास करने लगा। समाज में पंच मकार (मांस, मैथुन, मत्स्य, मद्य तथा मुद्रा) जैसी साधना का प्रचार होने लगा। अपने इस रूप में ये मत विकारों को प्रश्रय देने लगे तथा वाममार्गी हो गये। तंत्र-मंत्र, जादू-टोना तथा भोग-विलास को लेकर चलने वाले ये वाममार्गी ही बौद्ध-सिद्ध कहलाए तथा दूसरी तरफ धर्म,नियम संयम और हठयोग के द्वारा साधना के कठिन मार्ग पर चलने वाले नाथ सिद्ध के रूप में जाने गए पर अपने मूल रूप में ये दोनों ही बौद्ध थें, जो धीरे-धीरे बौद्ध धर्म के विकृत या परिवर्तित रूप में ढलते चले गये। इन तंत्र साधनाओं में स्त्री और शूद्र दोनों के लिए द्वार खुला था इसलिए जन सामान्य के बीच इसका प्रचार हुआ। फलस्वरूप जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव सभी संप्रदायों में तंत्रवाद का प्रभाव बढ़ गया था।[5][13][7][14][16][17][12]
सांस्कृतिक परिस्थिति
आदिकाल का आरंभ उस समय हुआ जब भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। दूसरी तरफ़ यह युग हिंदू-मुस्लिम संस्कृति के परस्पर मिलन का युग भी था। अतः यह वह युग था जब दो भिन्न संस्कृतियाँ आपस में मिल रही थी। संगीत, चित्रमूर्ति एवं भवन निर्माण इत्यादि कलाओं में लोग विशेष रुचि रखने लगे थें। हालांकि दूसरी तरफ़ इसी युग में महमूद गजनवी जैसे कई आक्रांता भारत आए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को क़ाफी क्षतिग्रस्त किया।[18][5][13][12] इस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों को लक्ष्य कर डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं-
आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है, वह परंपरागत गौरव से रहित तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। इस काल में हिंदू-संस्कृति धीरे-धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी। भारत के उत्सव मेलों, त्योहारों, वेश-भूषा विवाह तथा मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग मिलने लगा। यहाँ के गायन, वादन तथा नृत्य पर मुस्लिम छाप स्पष्ट दिखने लगा। भारतीय संगीत में सांरगी, तबला तथा अलगोजा जैसे वाद्यों का समावेश इसका स्पष्ट प्रमाण है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में जो थोड़ा-बहुत कार्य हुआ, उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। मूर्तिकला को छोड़कर अन्य भारतीय ललित कलाओं में मुस्लिम कला की कलम गहरे रूप में लगी।
इसी काल में भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, काँची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मन्दिरों का निर्माण प्रारम्भ हुआ था, ये मंदिर भारतीय संस्कृति के केंद्रबिंदु बने। अरब इतिहासकार अल-बेरुनी इन मंदिरों की भव्यता के विषय में लिखते हैं-
हिन्दू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुँच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण ही कर सकते हैं।[19]
साहित्यिक परिस्थिति
गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने के बाद और सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात् भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल-वैभव का केंद्र बन गया था। भारत के इसी क्षेत्र में कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अंहलवाड़ा आदि बड़ी-बड़ी राजधानियाँ थीं। इस क्षेत्र की भाषा का प्रचलन भी बढ़ गया था। अतः यह स्वाभाविक था कि उसी भू-भाग की जनता की चित्तवृत्ति के अनुरूप तत्कालीन साहित्य का निर्माण हुआ। उस समय के प्रमुख साहित्यिक सर्जक जो चारण कहलाते थें, भारत के पश्चिम में ही निवास करते थें। इसके अतिरिक्त पारस्परिक युद्ध तथा विदेशियों के निरंतर आक्रमणों के फलस्वरूप तत्कालीन समाज में एक प्रकार की अराजकता एवं अशांति की भावना उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में कविता के लिए युद्ध ही एकमात्र विषय बन गया था।[5][13][12] आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार-
सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी-साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई-भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बाते पीछे पड़ गई थी।[20]
इस युग के कवि राजाओं का आश्रय प्राप्त करने और धन की प्राप्ति के लिए अपने आश्रयदाताओं की भरपूर प्रशंसा किया करते थें। युद्ध का सजीव वर्णन करने के लिए ये कवि अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध में भी जाते थें। यही कारण है कि हिन्दी साहित्य के आदि युग में वीर रस की कविताएँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं।[5] आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हैं कि-
राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियो का समय बीत चुका था। राजदरबारों मे शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रणक्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था।[21]
पारस्परिक युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बलपूर्वक सुन्दर कन्याओं की प्राप्ति भी था। यह प्रवृत्ति आदिकाल में इतनी बलवती हो गई थी कि बिना रक्तपात के कोई स्वयंवर पूरा होता ही न था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का संघर्ष इस प्रवृत्ति का प्रतीक है।[5] इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर बुन्देलखण्ड के तत्कालीन सेनापति आल्हा लिखते हैं-
"जिहि की बिटिया सुन्दर देखी।
तिहि पर जाइ धरे हथियार॥"[22]
इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम यह हुआ कि कविगण आश्रयदाता के शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के साथ ही उन्हें सुन्दर कन्याओं के ऊपर आसक्त कराने के कर्त्तव्य का भी पालन किया करते थें। इसके लिए वे संबंधित सुंदरी के रूप का बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थें जिस कारण वीरता के साथ शृंगारिकता की प्रवृत्ति भी इस युग के काव्य में मिलती है।[5]
Remove ads
आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ
सारांश
परिप्रेक्ष्य
आदिकाल में एक ओर जहाँ कवियों द्वारा अपने-अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर काव्य रचे जा रहे थें तो वहीं दूसरी ओर सिद्धों, नाथों और जैनों के द्वारा भक्तिपरक काव्य भी रचे जा रहे थें। अतः इस युग के साहित्य को मूल रूप से रासो साहित्य और धार्मिक साहित्य दो भागों में बाँट कर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस युग में स्वच्छंद प्रवृत्ति से लौकिक साहित्य भी रचे गए। साथ ही गद्य साहित्य के भी कुछ आरम्भिक संकेत इस युग में मिलते हैं। हालांकि इस युग की प्रामाणिकता संदिग्ध है परंतु संदिग्ध होते हुए भी इसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषा में और गद्य-पद्य दोनों रूपों में रचना की प्रधानता इस युग में मिलती है।[23][24] इस युग की साहित्यिक प्रवृतियाँ इस प्रकार है-
वीर रस की प्रधानता
रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर रस से युक्त रचनाएँ इस युग में सर्वाधिक लिखी गई है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। इस काल के लेखक राजाओं पर निर्भर थें इसलिए उन्हें कई बार ना चाहते हुए भी राजा की वीरता व महानता को बढ़ा-चढ़ा कर वर्णित करना पड़ता था। जिससे राजा प्रसन्न होकर उन्हें प्रोत्साहन राशि देते थें। इस युग में गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, सोलंकी आदि राजा आपस में ही लड़ाई करते रहते थें। युद्ध करना ही एक मात्र धर्म बन गया था।[23][24] यही कारण है कि जगनिक लिखते हैं-
बारह बरिस लै कूकर जीऐं ,औ तेरह लौ जिऐं सियार,
बरिस अठारह छत्री जिऐं ,आगे जीवन को धिक्कार।[25]
इस काल में विदेशी आक्रमण के कारण भी निरंतर युद्ध हुआ करते थें इसलिए भी इस काल में वीर रसात्मक ग्रंथों का आधिक्य है। इन वीर रसात्मक ग्रंथों के कुछ उदाहरण है- पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, बीसलदेव रासो आदि।
युद्ध-वर्णन में सजीवता
रासो ग्रंथों में किये गये युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ-जहाँ युद्धवर्णन के प्रसंग हैं, वहाँ-वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आँखों देखा हाल सुना रहा है। इस युग के चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थें, अतः अवसर पड़ने पर वे अपने-अपने आश्रयदाता के साथ रणक्षेत्र में जाकर युद्ध भी लड़ते थें। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था, अतः इन युद्धवर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है, वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपितु योद्धाओं के उमंगों, मनोदशाओं एवं क्रियाकलापों का भी सुंदर वर्णन किया है। इन युद्ध-प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी, अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थें।[23][24] इनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा हैं,
"देश पर सब ओर से आक्रमण की सम्भावना थी। निरन्तर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थें। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना-योजना का अविष्कार।"[26]
पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध-वर्णनों के कारण ही एक सशक्त रचना मानी जाती है।
प्रामाणिकता का अभाव
आदिकाल के अधिकांश रासो काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बतायी गई है, वह भी अप्रामाणिक मानी गई है।[23][24] आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
"इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएँ और कुछ संवत तो ठीक होते।"[27]
ऐतिहासिकता का अभाव
इस युग के वीर रसात्मक ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध हैं। रासो साहित्य के चरित्र नायक भले ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं किन्तु इन काव्य-ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। इन ग्रंथों में तथ्य कम और कल्पना अधिक है। परिणामतः इनके माध्यम से अनेक ऐतिहासिक भ्रांतिया उत्पन्न होती है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किये हैं, वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। अपने आश्रयदाता की तुलना अद्भुत, अलौकिक शक्तियों के साथ करना इन कवियों की जरूरत थी। कल्पना के द्वारा इन कवियों ने प्रत्येक वस्तु को रंगीन और अद्भुत बनाने का प्रयास किया हैं। इस युग के काव्य में साधारण घटना भी चमत्कारपूर्ण बना दी जाती थी। घटनाओं, नामावली तिथियों का जो विवरण रासो काव्यों में उपलब्ध होता है, वह इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है, उससे ये ग्रंथ मेल नहीं खाते। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए कई काल्पनिक वर्णन किये हैं, यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है।[23][24]
शृंगार रस की प्रधानता
इस काल में वीर रस के साथ शृंगार रस का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इस युग में कई युद्ध सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से लड़े जाते थें, अतः शृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश इन काव्य ग्रंथों में होना स्वाभाविक है। इस युग के कवियों ने राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नख-शिख परिपाटी पर किया है। इन वर्णनों से प्रसन्न हो कर राजा अक्सर कवियों को पुरस्कृत किया करते थें। नायिका के रूप-सौंदर्य के साथ-साथ उनके वयः संधि का भी सुंदर वर्णन रासो ग्रंथों में किया गया है। बीसलदेव रासो में संयोग-वियोग दोनों शृंगार रूपों का सुंदर प्रयोग हुआ है।[23][24] पृथ्वीराज रासो के शृंगार रस से युक्त एक पंक्ति का उदाहरण इस प्रकार है-
मनहुँ कला ससभान कला सोलह सो बन्निय।
बाल वैस, ससि ता समीप अम्रित रस पिन्निय॥[28]
इन कवियों के शृंगारिक वर्णन को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं-
उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु, कन्याहरण का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था। रणक्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था।[21]
आश्रयदाताओं की प्रशंसा
आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं व सामंतों के आश्रय में रहते थें। उनको आश्रय तभी प्राप्त होता था जब वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थें। ये रचयिता चारण कहे जाते थें जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य समझते थें। अपने आश्रयदाता की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारण कवियों की प्रमुख विशेषता थी। इन कवियों का आमजन से कोई विशेष लगाव नहीं था। जनता से रचना का संबंध सिर्फ श्रोता का रह गया था। प्रत्येक रचना राजा को खुश करने के लिए की जाती थी। जनता के कष्टों से कवियों का कोई लेना देना नहीं था। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश एवं वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचनाएँ हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है।[23][24]
राष्ट्रीय एकता का अभाव
आदिकाल में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। यही कारण है कि इस काल में वीरता का वर्णन तो बार-बार हुआ है, परन्तु उस वर्णन में स्वदेश अभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड-खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे-छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संषर्ध में रत रहते थें। ये राजा दस-बीस गाँवों के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थें। चूँकि इस समय के कवि राजाश्रय में जीवन यापन करते थें इसलिए कवि भी अपने राजा के अलावा शेष राजाओं को नीचा दिखाने के लिए काव्य रचते थें और अपने राजा की झूठी सच्ची बातों को बढ़ा-चढ़ा कर उन्हें चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने में कोई संकोच महसूस नहीं करते थें। कवि जनता से अलग रहने के कारण सामंती वैभव एवं ऐश्वर्य का वर्णन अधिक मात्रा में करते थें। अतः इस काल के कवि भी सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थें। इस काल में प्रजा अपने राजा के अधिकार क्षेत्र को ही देश मानती थी और उसके प्रति अपनी पूरी आस्था और निष्ठा रखती थी, साथ ही पड़ोसी राज्य को वे शत्रु राष्ट्र समझते थें। अतः इस युग में सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। परिणामतः विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में भी वे विफल हुए। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंचमात्र भी विचलित नहीं होते थें। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे-धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पराजित हो गए।[23][24]
अतिशय कल्पना बोध
इस युग के चारण कवियों की रचनाएँ तथ्य परक न होकर कल्पना प्रधान होती थी। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं पर इनमें इतिहास नाममात्र का ही है। इन कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में ऐतिहासिक सत्य की अवहेलना भी कर दी है। इन वीरगाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएँ कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है।[23][24] इस विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा हैं-
"बात संवत् ही तक नहीं है। इतिहास-विरुद्ध कल्पित घटनाएँ जो भरी पड़ी हैं उनके लिये क्या कहा जा सकता है? माना कि रासो इतिहास नहीं हैं, काव्य-ग्रंथ है। पर काव्य-ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलट-फेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज-विजय भी तो काव्य-ग्रंथ ही है; फिर उसमें क्यों घटनाएँ और नाम ठीक ठीक हैं?"[27]
विविध छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग
इस युग के ग्रंथों में छंदों की विविधता स्पष्ट परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है न पूर्ववर्ती साहित्य में। दोहा, गाथा, पद्धरि, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया आदि इस युग के प्रचलित छंद हैं। इन छंदो का प्रयोग मात्र कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव-प्रकाशन के लिए भी किया जाता था।[23][24] पृथ्वीराज रासो में तो 10,000 से अधिक छंद हैं।[29] आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रासो ग्रंथों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा हैं-
"रासो के छंद जब बदलते है तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कम्पन उत्पन्न करते हैं।[30][31]
इस युग की रचनाओं में अतिशयोक्ति अलंकार का बहुधा प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का चित्रण भी इन काव्य ग्रंथों में मिलता है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग बहुधा हुआ है।[23]
भाषा शैली
इस काल के साहित्य में हमें मूल रूप से अपभ्रंश, डिंगल-पिंगल, मैथिली और खड़ी बोली चार भाषाओं के प्रयोग दिखते हैं।
- अपभ्रंश
यह भाषा योग मार्ग के बौद्धों की रचनाओं में, नाथपंथियों के प्रचार-ग्रंथों में, जो मूलतः राजपूताना तथा पंजाब की प्रचलित भाषा में लिखे गये हैं और जैन आचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभु सूरि आदि के ग्रंथों में प्रयुक्त मिलती है। विद्यापति ने भी अपभ्रंश में छोटे-छोटे ग्रंथों की रचना की है। सिद्धों के द्वारा प्रयुक्त अपभ्रंश में पूर्वी प्रभाव तथा जैन साहित्य में नागर अपभ्रंश का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। इन ग्रंथों में चरित्र, रासक, चतुष्पदी ढाल, दूहा आदि छंदो का प्रयोग हुआ है। विषय की दृष्टि से तांत्रिक साहित्य, वीरगाथा साहित्य, श्रृंगार काव्य तथा दर्शन साहित्य का आरंभिक रूप अपभ्रंश के ही अंतर्गत दिखाई देता है। वस्तु-स्थिति यह है कि उस समय के कवियों की बहुप्रचलित भाषा अपभ्रंश ही थी। सिद्धों और नाथों की कृतियों में देश-भाषा-मिश्रित अपभ्रंश का रूप प्राप्त होता है। इस भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल (अंतिम समय में) में प्रचलित थी। अपभ्रंश के इस संध्या भाषा रूप से ही पुरानी हिंदी जिसे ब्रज और खड़ी बोली जैसे काव्य-भाषा का ढाँचा कहा गया है, पनपी है। अपभ्रंश भाषा जैसे-जैसे देशभाषा की ओर बढ़ती गई, इसमें संस्कृत, तत्सम और तद्भव शब्दों के प्रयोगों को अधिकाधिक स्थान प्राप्त होता गया। अरबी-फारसी के शब्द भी प्रचलन में आने लगे।[32][33][5]
- डिंगल और पिंगल
प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रजभाषा तथा मध्य देश की भाषा के संयोग से जो भाषा बनी वह पिंगल कहलाई जबकि अपभ्रंश भाषा से युक्त बोलचाल की राजस्थानी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका विशेष स्थान है। पिंगल भाषा में फारसी, अरबी, तुर्की के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। डिंगल और पिंगल का मिश्रित रूप वीरगाथाओं में दिखाई देता है। भाषा की दृष्टि से डिंगल साहित्य बहुत ही अव्यवस्थित है। विशेष रूप से परवर्ती परिवर्तनों के कारण इसके शुद्ध रूप का पता लगाना कठिन है। पिंगल के अतिरिक्त डिंगल में अपभ्रंश के प्रभाव के कारण संयुक्ताक्षरों और अनुस्वारों की अधिकता हो गई है। इस कारण से डिंगल भाषा कुछ-कुछ कृत्रिम लगती है। चारण कवियों ने डिंगल और पिंगल दोनों का साथ-साथ प्रयोग किया है। वस्तुतः डिंगल राजस्थानी की रचना शैली की भाषा है और पिंगल ब्रजभाषा की रचना शैली की भाषा।[34][35][36]
- मैथिली भाषा
मैथिली बिहार में प्रयुक्त एक बोली है और यह हिंदी की एक विभाषा मानी जाती है। यही कारण है कि विद्यापति की पदावली को हिंदी का ग्रंथ माना जाता है। आदिकालीन ग्रंथों में विद्यापति की पदावली का विशेष स्थान है।[37][38]
- खड़ी बोली
अमीर खुसरो के काव्य में जनता की उस बोली के दर्शन होते हैं जो कालांतर में विकसित होकर खड़ी बोली कहलाई। तत्कालीन जनभाषा के दर्शन खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में मिलता है। यह दिल्ली और मेरठ की आस-पास की भाषा थी। इस भाषा की क्रियाएँ हिंदी की हैं, साथ ही इसमें अरबी-फारसी के भी काफी शब्द मिलते हैं।[39][24]
Remove ads
आदिकालीन साहित्य
सारांश
परिप्रेक्ष्य
आदिकालीन साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहला धार्मिक साहित्य, जिसमें मूलतः सिद्ध, नाथ और जैन कवियों द्वारा रचित साहित्य आता है। इस साहित्य की रचना मुख्य रूप से अपने-अपने धर्मों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से किया गया था। दूसरा रासो साहित्य, जिसकी रचना चारण कवियों के द्वारा अपने-अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके अतिरिक्त इस काल में कुछ मात्रा में लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य की भी रचना हुई है।
सिद्ध साहित्य
बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थें। बौद्धमत को मानने वाले आरंभ में ईश्वर की भक्ति का विरोध करते थें, लेकिन धीरे-धीरे वे ही बुद्ध को भगवान के रूप में पूजने लगें और जब बौद्ध धर्म में तांत्रिक सिद्धों का प्रभाव बहुत बढ़ गया, तो यह धर्म अपने वास्तविक रूप और दिशा से एकदम अलग हो गया। आठवीं शताब्दी के आस-पास इन तांत्रिक सिद्धों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। इन्होंने बौद्ध धर्म के त्याग और संयम के स्थान पर भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया था। शराब पीना और निम्न वर्ग की स्त्रियों को योगिनी कहकर उनके साथ भोग विलास करना आवश्यक समझा जाने लगा था। मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन और मुद्रा, इन पाँच मकारों का सेवन इनकी साधना का प्रमुख अंग बन गया था। सिद्धों के चमत्कारों का नारी-समाज पर इतना प्रभाव पड़ा कि स्त्रियाँ लोक-लाज, कुल मर्यादा को छोड़कर विपरीत दिशा में जाने लगी। धर्म के नाम पर समाज में वासना अबाध गति से फूट कर बाहर निकल पड़ी। इन क्रियाओं का प्रयोग ही निर्वाण प्राप्ति समझा जाने लगा। मन के निर्विकार और निश्चल स्थितियों के लिए महासुख और सहजयान को प्रधानता दी जाने लगी। इन्होंने निर्वाण साधना या महासुख का वर्णन बड़ी अश्लील वाणी में किया हैं। अपनी इस महासुख अवस्था को ये समरस अवस्था भी कहते थें और अपनी खुली भाषा में आध्यात्मिक पुट देकर उसकी व्याख्या करते थें। इन सहजयानी सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इनमें कुछ संस्कृत के अच्छे विद्वान थें। साहित्यिक योगदान की दष्टि से सिद्धों का साहित्य दोहा या दूहा नामक मुक्तक रूप में मिलता है। सिद्धों की नीति, रीति, शृंगार एवं धर्म संबंधी मान्यताएँ हिंदी के आदिकाल को तो विशेष प्रभावित नहीं करती पर संत साहित्य को अवश्य ही प्रभावित करती है, जिसे सिद्धों का योगदान माना जा सकता है।[40] सिद्ध साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी। सरहप्पा (सरोजपाद अथवा सरोजभद्र) प्रथम सिद्ध कवि माने गए हैं। इसके अतिरिक्त शबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कण्हपा, कुक्कुरिपा आदि सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं।[24][23][5][41][42][7]
- सिद्ध साहित्य की विशेषता
- सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है।
- सिद्ध साधना पद्धति में शिव-शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती थी।
- सिद्ध साहित्य में जाति प्रथा एवं वर्णभेद व्यवस्था का विरोध किया गया है।
- इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया है।
- सिद्धों में पंच मकार (मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन) की दुष्प्रवृति देखने को मिलती है। हालांकि तंत्रशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न बताया गया है।
- भाषा के विकास की दष्टि से सिद्धों द्वारा प्रस्तुत अपभ्रंश भाषा ने हिंदी में महत्त्वपूर्ण योगदान निभाया है। क्योंकि 'संध्याभाषा' की शब्दावली से बहुत से शब्द-रूप कबीर आदि संतों की बानियों में प्रयुक्त किए गये हैं।
- शैली की दृष्टि से सिद्ध साहित्य के मुक्तक काव्य से दूहा या दोहा, पद, चर्चा गीत तथा रहस्यात्मक उक्तियों से हिंदी में दोहा पद तथा गीति काव्य रूपों का प्रयोग, विद्यापति तथा संत कवियों ने खूब किया है।
- दार्शनिक अथवा रहस्यात्मक दष्टि से सिद्ध-साहित्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा बौद्ध धर्म के शून्यवाद को मिलाकर शरीर में ही सारी सिद्धियों का स्रोत बताया है और उसका उपभोग करने की सलाह दी है।
- सिद्ध-साहित्य ने संत-साहित्य को विशेषतः कबीर, दादू तथा रविदास आदि कवियों को रहस्यवाद के क्षेत्र में तथा उलट-बांसियों के क्षेत्र में बहुत प्रभावित किया है।
नाथ साहित्य
सिद्धों की वाममार्गी भोगप्रधान योगसाधना की प्रतिक्रिया स्वरुप नाथ पंथी का आरंभ हुआ। नाथ पंथ के साधक हठयोग की साधना करते थें। राहुल सांकृत्यायन नाथों को सिद्धों की परम्परा का ही विकसित रूप मानते हैं। इस पंथ के प्रवर्तक मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ माने गए हैं। इनका समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। नाथ पंथ के लिए सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योगमार्ग, योगसम्प्रदाय, अवधूतमत एवं अवधूत-सम्प्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। सिद्ध लोग जहाँ नारी भोग में विश्वास करते थें, वहीं नाथ पंथी उसके विरोधी थें। नाथ सम्प्रदाय ने नारी की एक प्रकार से निंदा की है और उन्हें माया के समतुल्य माना है। वामाचार के विरुद्ध इन्होंने पवित्र योगसाधना का विकास किया है। इन्होंने सिद्धों की बहिर्वर्ती साधना के विपरीत अन्तःसाधना पर बल दिया। पतंजलि के योगदर्शन का आधार लेकर इन्होंने हठयोग दर्शन को विकसित किया। इन्होंने षटचक्रभेदन, कुंडलिनी जागरण तथा नादबिन्दु की साधना को महत्त्वपूर्ण माना। हठयोग की जटिलता तथा साधना पद्धति की कठिनाइयों के कारण इनकी साधना में गुरु का काफ़ी महत्व दिखाई देता है। नाथ पंथ जीवन के प्रति सहज और संतुलित दृष्टि को अपनाने के पक्षधर रहे हैं। सामाजिक एवं आध्यात्मिक अतिचारों-अतिवादों का इन्होंने विरोध किया है। पश्चिम भारत में प्रचार-प्रसार के कारण नाथ पंथियों की भाषा ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी एवं हरियाणवी से प्रभावित है। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। वे मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थें। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय 845 ई॰ माना जाता है। डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं सदी का कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें 13वीं सदी तथा डॉ॰ पीतांबर दत्त बड़थ्वाल उन्हें 11वीं सदी से संबंधित मानते हैं। गोरखनाथ की कुछ रचनाएँ इस प्रकार हैं-सबदी, पद, प्राण-संकली, सिध्यादरसन, नरवै-बोध, अभैमात्राजोग, आत्मबोध पन्द्रह तिथि, सप्तवार, मछिन्द्र गोरख बोध, रोमावली, ग्यानतिलक, ग्यानचौतीसा एवं पंचपात्रा। डॉ॰ पीतांबर दत्त बड़थ्वाल ने गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है। नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योगदान दिया, उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी, जालंधरापम आदि प्रमुख हैं। नाथों की कुल संख्या 9 मानी गई है।[24][23][5][41][43][7]
- नाथ साहित्य की विशेषता
- नाथों साहित्य के जरिये सामंती भोगमूलक समाज में योग तथा संयम का प्रसार हुआ।
- इन्होंने हिंदू-मुस्लिम दोनों की सहभागिता पर बल दिया।
- नाथ हठयोग में विश्वास करने वाले और हठयोगी साधना द्वारा शरीर एवं मन को शुद्ध कर शून्य में समाधि लेने वाले थें।
- इन्होंने ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है।
- इन्होंने मनोविकारों और भोग विलास की भरसक निंदा की है।
- नाथ पंथी कवियों ने नारी को माया मानकर उनसे दूर रहने को कहा है।
- इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है।
- इस साहित्य से हठयोग का उपदेश प्राप्त होता है।
- इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है।
- इन्होंने मन, प्राण, शुक्र, वाक्, और कुंडलिनी इन पांचों को संयम में रखने के तरीकों को हठयोग कहा है।
- इस साहित्य में भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से मिलती है।
- नाथ साहित्य में साधनात्मक शब्दावली का प्रयोग भी बहुलता में मिलता है।
जैन साहित्य
जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने जैन धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाता है। आदिकालीन जैन साहित्य की रचना अवधि 8वीं से 13वीं शती तक मानी गयी है। हालांकि कुछ जैन साहित्य 19वीं शती तक भी मिलते हैं। जैन साहित्य में पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथाकाव्य, रासकाव्य एवं रहस्यवादी काव्य लिखे गये हैं। इसके अलावा व्याकरण ग्रन्थ, श्रृंगार, शौर्य, नीति और अन्योक्ति संबंधी फुटकर पद्य भी इनमें लिखे गये हैं। जैन कवियों की रचनाएँ आचार, रास, फागु चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। जैन साहित्य का महत्व केवल जैन धर्म के प्रतिपादन की दृष्टि से ही नहीं, वरन् भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी है। जैन साहित्य के प्रारंभिक रचनाओं में अपभ्रंश का प्रचलित रूप अधिक पाया गया है। प्रारम्भिक जैन साहित्य में दोहा-चौपाई पद्धति पर चरित्र काव्य या आख्यानक काव्य का निर्माण हुआ है। यही परम्परा आगे चलकर सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई। डॉ॰ लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने लिखा हैं,
जैनधर्म की दोहा-चौपाई पद्धति आगे चलकर सूफी कवियों, तुलसी आदि द्वारा अपनाई गई। इन प्रारंभिक रचनाओं के आधार पर ही पुरानी हिंदी का जन्म और पीछे खींच ले जाया जाता है।[44]
जैन धर्म के दो प्रधान संप्रदायों-दिगंबर और श्वेतांबर में से दिगंबर सम्प्रदाय से संबंधित रचनाएँ पुरानी हिंदी में अधिक पाई गई हैं जबकि श्वेतांबर संप्रदाय संबंधी रचनाएँ गुजराती में अधिक पायी गई हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र आदि जैन साहित्य के प्रख्यात कवि हैं। जैनों का संबंध राजस्थान तथा गुजरात से विशेष रूप से रहा है, इसीलिए अनेक जैन कवियों की भाषा प्राचीन राजस्थानी भी रही है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। इन्होंने जैन तीर्थंकरों के जीवनचरित तथा वैष्णव अवतारों की कथाओं को जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध किया है। आदिकालीन जैन साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1184 ई॰ में शालिभद्र सूरि ने की थी।[24][23][5][41][45][7]
- जैन साहित्य की विशेषता
- जैन साहित्य के अनुसार ईश्वर सृष्टि निर्माता नहीं हैं। वह चित् एवं आनंद का स्रोत हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना और पौरूष से परमात्मा का रूप धारण कर सकता है।
- जैन साहित्य ने समाज में ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह का ख़ूब प्रचार-प्रसार किया।
- प्रारम्भिक जैन साहित्य में दोहा-चौपाई पद्धति पर चरित-काव्य या आख्यानक काव्य का निर्माण हुआ। यही परम्परा आगे चलकर सूफी कवियों द्वारा ग्रहण की गई।
- इनका साहित्य मूलतः धर्म-प्रचार का साहित्य है, किन्तु साहित्यिक सौष्ठव के अंश इनमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं।
- तत्कालीन व्याकरणादि ग्रंथों में इस साहित्य के उद्धरण मिलते हैं।
- जैन कवि स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल आदि ने रामायण और महाभारत की कथाओं के नायक राम और कृष्ण के चरित्र को अपने धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों के अनुरूप अंकित किया है।
- जैन तीर्थकारों एवं महापुरूषों के चरित्र संबंधी कथानक भी जैन साहित्य में लिखे गये हैं तथा लोक-प्रचलित प्रसिद्ध नैतिकतावादी आख्यान भी जैन धर्म के रंग में रंग कर प्रस्तुत किये गये हैं।
- जैन साहित्य में शांत रस की प्रधानता पाई जाती है।
चारण-साहित्य
चारण जाति ने विभिन्न क्षेत्रों में कई उत्कृष्ट कवि, इतिहासकार, योद्धा, निष्ठावान राजदरबारी और विद्वान प्रदान किए हैं। चारण काव्य सदृढ़ रूप से 8-10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उपलब्ध हैं। अनगिनत संख्या में गीत, दोहे, समग्र रचनाएँ, ऐतिहासिक लेखन, और कई अन्य छंद और गद्य रचनाएँ चारण साहित्य का भाग हैं। पिछली छह शताब्दियों के दौरान उनके लेखन का निरंतर प्रवाह रहा है। इतिहासकारों में सूर्यमल्ल मिश्रण, कविराजा बाँकीदास, कविराजा दयालदास और कविराजा श्यामलदास इस क्षेत्र के दिग्गज हैं। चारण शैली के लेखकों ने केवल एक रस में ही नहीं, बल्कि एक ही समय में वीर काव्य, श्रृंगार काव्य और भक्ति काव्य में लिखकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।[46] चारण साहित्य का वीर काव्य योद्धाओं को अपनी भूमि, धर्म, नारी और उत्पीड़ितों के सम्मान के लिए मरते दम तक संघर्ष करने को प्रेरित करता है।[47]
चारण कवियों ने अपने साहित्य में डिंगल (प्राचीन राजस्थानी), संस्कृत, पिंगल (डिंगल से प्रभावित ब्रजभाषा), अपभ्रंश, राजस्थानी (मारवाड़ी, मेवाड़ी, आदि) व गुजराती के साथ-साथ उर्दू-फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। चारणों के अलावा, इनके हठधर्मी दृष्टिकोण का पालन अन्य समकालीन कवियों, जैसे भाट, ब्राह्मण, ढाढ़ी, सेवग (मग-ब्राह्मण), राजपूत, मोतीसर, रावल, पंचोली (कायस्थ) और अन्य लोगों ने भी किया, जिनमें जैन धर्म के लोग भी शामिल थे, और चारण साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक बहुत ही जीवंत और सशक्त साहित्य था, और इसीलिए इसने पश्चिमी-भारत की रेगिस्तानी भूमि और इसके नायकों के भाग्य को आकार देने और ढालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[47]
चारणो ने साक्षात् अनुभव के द्वारा वीरकाव्य का सृजन किया है। वे कलम के ही नहीं, तलवार के भी धनी थे । फलतः संस्कृत के प्रशस्तिमूलक काव्य जहाँ ऐतिहासिक अनुसंधान और विद्वद् मंडली की संपत्ति बन गये, वहाँ रासो जनता की निधि बन गया। एक बँधे कूप की तरह हो गया, दूसरा बहती गंगा की तरह; और तभी विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने चारणों की काव्य-कला पर मुग्ध होकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है ।[51] 'राजस्थान रिसर्च सोसाइटी' में दिये गये भाषण में टैगोर कहते हैं —
भक्ति साहित्य हमें प्रत्येक प्रांत में मिलता है । सभी स्थानों के कवियों ने अपने ढंग से राधा और कृष्ण के गीतो का गान किया है। परन्तु अपने रक्त से राजस्थान ने जिस साहित्य का निर्माण किया, वह अद्वितीय है और उसका कारण भी है। चारणों ने अपनी कठोर वास्तविकता का स्वयं सामना करते हुए युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि के साथ स्वाभाविक काव्य-गान किया है । उन्होने अपने सामने साक्षात् शिव के ताण्डव की तरह नृत्य देखा था । क्या आज कोई कल्पनाशक्ति से उस प्रकार का काव्य रच सकता है? राजस्थानी भाषा के हर छोटे से गीत में निहित वीर भावना और तरंग, राजस्थान की मूल संपत्ति है, और बड़े पैमाने पर भारत का गौरव है। यह सहज, शुद्ध और प्रकृति के करीब है। मैने कई बार सुना था कि चारण अपने काव्य से वीर योद्धाओं को प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया करते थे। आज मैंने उस सदियों से पुरानी कविता का स्वयं अनुभव किया है। उसमें आज भी बल और ओज है।[52]
रासो साहित्य
आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य की एक विशिष्ट परंपरा देखने को मिलती है। सामान्यतः रासो काव्य से वीरगाथात्मक काव्य का बोध होता है। इसकी रचना भट्ट और चारण कवियों द्वारा की गई है। रासो साहित्य तत्कालीन जनमानस की अभिव्यक्ति नहीं है। यह सामंती समाज की उपज है इसलिए रासो साहित्य के कथानक की बनावट भी सामंतों के मनोनुकूल है। आदिकाल में केंद्रीय सत्ता के अभाव में राजाओं के मध्य शक्ति प्रदर्शन के लिए अधिकाधिक संघर्ष हुआ करते थें। रासो साहित्य उन्हीं संघर्षों की कथा कहती है। साथ ही इनमें वीरगीतों के साथ प्रेम प्रसंगों की चर्चा भी की गई है। रासो साहित्य एक तरह का प्रशस्तिगान है जिनमें चारण कवि अधिकतर अपने आश्रयदाता या सामंतों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थें। इनकी विषय-वस्तु अत्यंत सीमित है। सामंतों के जीवन में दो बातों की प्रधानता थी- पहला युद्ध और दूसरा प्रेम। इसलिए चारण कवियों के इस साहित्य में भी इन्हीं दो विषयों की प्रमुखता देखने को मिलती है। व्यवस्था से शोषित सामान्य मानव के घरेलू जीवन और उसकी समस्याओं की ओर इन कवियों का ध्यान नहीं गया है।[53][54][23][5][41][4][7][6]
- रासो शब्द की व्युत्पत्ति
रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है[55]-
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बीसलदेव रासो में प्रयुक्त रसायन शब्द ही कालांतर में चलकर रासो बना।
- मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस ग्रंथ में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध तथा वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो, उसे ही रासो ग्रंथ कहते हैं।
- गार्सा द तासी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से हुई है।
- रामचंद्र वर्मा के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से हुई है।
- मुंशी देवीप्रसाद के अनुसार रासो शब्द का अर्थ है- कथा जिसका एकवचन रासो तथा बहुवचन रासा है।
- जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति राजादेश शब्द से हुई है।
- गौरीशंकर ओझा के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रास शब्द से हुई है।
- पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से हुई है।
- विश्वनाथप्रसाद मिश्र के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति का आधार रासक शब्द है।
- बैजनाथ खेतान के अनुसार रासो शब्द का अर्थ है- झगड़ा, पचड़ा या उद्यम। इसी कारण से इस साहित्य का नाम रासो साहित्य पड़ा।
- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो तथा रासक शब्द एक-दूसरे के पर्याय हैं। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी। आदिकाल में रचित वीरगाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित-काव्यों के लिए किया है। कालांतर में इसी रासक शब्द से रासो शब्द बना।
- डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त के अनुसार विविध प्रकार के रास, रासावलय, रासा और रासक छंदों, नाट्य-रासक, उपनाटकों आदि से रासो-प्रबंध परम्परा का संबंध रहा है।
- रासो साहित्य की विशेषता
- रासो साहित्य में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है।
- रासो साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया है।
- रासो साहित्य में ऐतिहासिकता के साथ-साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है।
- रासो साहित्य में युद्ध और प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है।
- रासो साहित्य में वीर रस एवं शृंगार रस की प्रधानता है।
- रासो साहित्य में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है।
- रासो साहित्य में विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है।
- रासो और रास साहित्य में अंतर
आदिकालीन साहित्य में रास ग्रंथ और रासो ग्रंथ दोनों प्रकार की रचनाओं की चर्चा मिलती है। रास साहित्य और रासो साहित्य में मुख्य अंतर भावानुभूति के धरातल पर है। रास साहित्य की संवेदना धार्मिक अनुभूति अथवा लौकिक प्रेम की अनुभूति से जुड़ी हुई है। रास काव्य का प्रसार जैन साहित्य में देखने को मिलता है। रास साहित्य में लौकिक प्रेमानुभूति की भी अभिव्यक्ति हुई है। संदेश रासक इसी तरह के साहित्य का उदाहरण है। आदिकालीन साहित्य में रास काव्य का नाम जैन रचनाकारों द्वारा लिखे गए रासक ग्रंथों और संदेश रासक जैसे प्रेमानुभूति प्रधान काव्य संवेदना के लिए रूढ़ है। अतः रासो काव्य धारा ने जहाँ युद्ध और प्रेम के पक्षों तक अपनी संवेदना को सीमित रखा, वहीं रास काव्य में जीवन के विविध पक्षों का चित्रण मिलता है। डॉ॰ गणपति चंद्र गुप्त ने मुनि शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिन्दी का प्रथम रास काव्य माना है।[56][23][54][57][55]
लौकिक साहित्य
लौकिक साहित्य के अंतर्गत उन रचनाओं को रखा जाता है, जो उपलब्ध तो हैं और जिनके प्रणेताओं के बारे में भी बहुत कुछ ज्ञात है किन्तु पाठ, काल, तिथि आदि की दृष्टि से वे संदेहास्पद हो। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने इसे संदिग्ध साहित्य की संज्ञा दी है। आदिकाल में जहाँ एक तरफ़ धार्मिक साहित्य और रासो साहित्य प्रयाप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ़ इनसे भिन्न एक दूसरे प्रकार की साहित्यिक लोकधारा भी प्रवाहशील थी। साहित्य की यह लोकधारा तत्कालीन लोकभाषा में उपलब्ध थी। हालांकि चारण कवियों के साहित्य की तरह इस साहित्य को राजाश्रय नहीं मिला। इसी कारण लौकिक साहित्य ने जीवन की रची-बसी विषय-वस्तु को अपने साहित्य का विषय बनाया। इस साहित्य में अलंकरण के प्रयोग की जगह जीवन की स्वाभाविक दशाओं का वर्णन है। लौकिक साहित्य के विभिन्न अंग केवल शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ही अध्ययन के विषय न होकर सांस्कृतिक अर्थात् मानव विज्ञान तथा समाजशास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में मुलतान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला से अधिक मात्रा में लौकिक साहित्य प्राप्त हुए हैं। जिसके परिणामस्वरूप इन लौकिक साहित्य में वहाँ के स्थानीय भाषा और संस्कृति का अधिकाधिक प्रभाव है। कुछ प्रसिद्ध लौकिक साहित्य के रचनाकार जैसे, संदेश रासक के कवि अब्दुल रहमाण मुलतान के थें। ढोला मारू रा दूहा[58] जो एक प्रसिद्ध लौकिक साहित्य है, उसके रचयिता कल्लौल राजस्थान से थें। अमीर खुसरो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थें। उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा अवध के रहने वाले थें। विद्यापति तथा ज्योतिरीश्वर ठाकुर मिथिला के निवासी थें।[23][5][41][4]
आदिकालीन गद्य साहित्य
आदिकाल में पद्य रचनाओं के साथ-साथ कुछ गद्य रचनाएँ भी देखने को मिलती है। हालांकि आदिकाल में जो गद्य साहित्य मिलता है वह व्याकरण और शास्त्र की सीमाओं के खंडन-मंडन तक ही सीमित है। इस काल की तीन उल्लेखनीय गद्य रचनाएँ हैं रोडा की कृति "राउलवेलि" या "राहुल खेल" दामोदर शर्मा की कृति उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्णरत्नाकर।[24][5][41]
Remove ads
हिंदी का प्रथम कवि
हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है।[5] विभिन्न इतिहासकारों व विद्वानों के अनुसार हिंदी का पहला कवि निम्नलिखित बताया गया हैं-
- डॉ॰ रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू (६९३ ई॰) हैं।
- राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहपा (७६९ ई॰) हैं।
- शिवसिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि पुष्पदंत या पुण्ड (१०वीं शताब्दी) हैं।
- चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि राजा मुंज (९९३ ई॰) हैं।
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि राजा मुंज व भोज (९९३ ई॰) हैं।
- गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूरि (११८४ ई॰) हैं।
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि अब्दुल रहमान (१३वीं शताब्दी) हैं।
- बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि विद्यापति (१५वीं शताब्दी) हैं।
Remove ads
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads